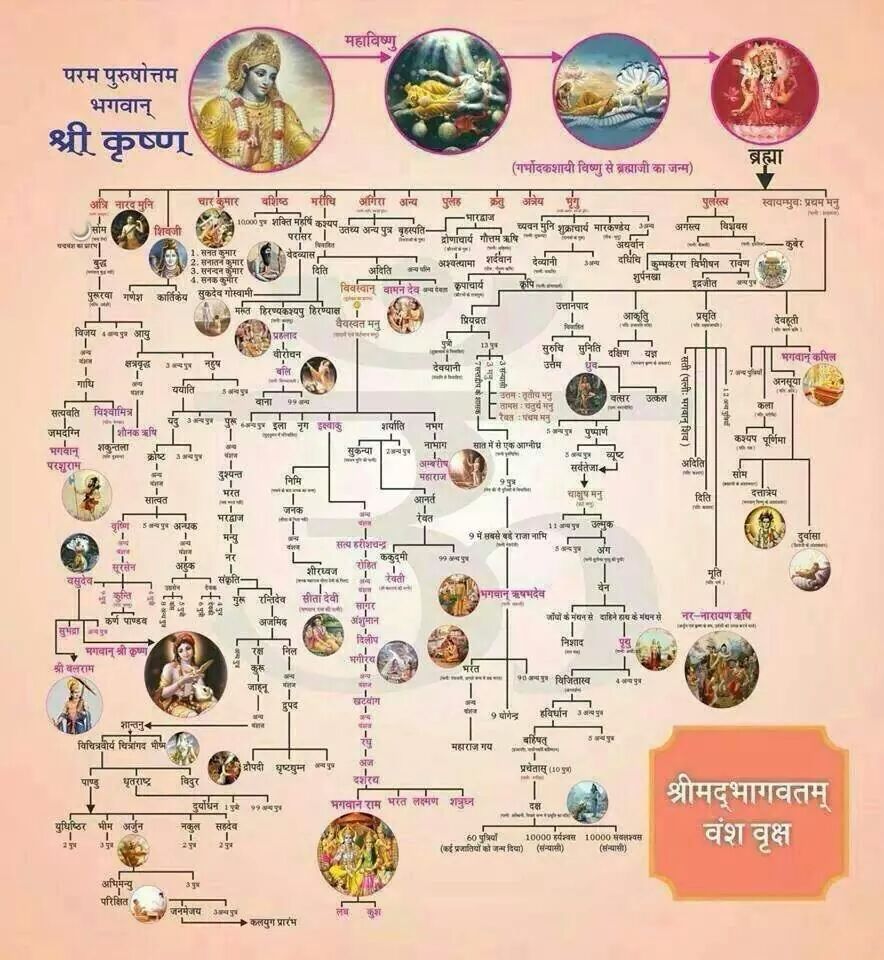उपन्यास-चर्चा क्या मोनालीसा वाकई हंस रही थी?
मोनालीसा हंस रही थी (उपन्यास), लेखक: अशोक भौमिक, पृष्ठ: १२७, कीमत: रु ११० (पेपरबैक), अंतिका प्रकाशन, सी-५६/यू जी ऍफ़-४, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-II, गाजियाबाद-२०१००५.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अशोक भौमिक जी, एक बड़े कलाकार हैं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, इतने बड़े मर्मज्ञ कि उनकी कला साधना पर चर्चा करना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा.
वह बड़े लेखक भी हैं, तब तक मैं नहीं जानता था. कुछ समीक्षाएं देखी तो लगा कि “मोनालीसा हंस रही थी” वास्तव में अच्छी कृति होगी. बाद में स्वयं भौमिक जी ने उसे पढने का सुझाव भी दिया था. अंतिका प्रकाशन की वेबसाईट पर अशोक भौमिक सर की कई अन्य पुस्तकें भी सुशोभित थी. कुछ विशुद्ध कला की, कुछ साहित्य-- उपन्यास और कहानी संग्रह थे. “आईस पाईस (कहानी संग्रह), “बादल सरकार: व्यक्ति और रंगमंच”, और “समकालीन भारतीय चित्रकला: हुसैन के बहाने” कुछ उनकी अन्य पुस्तकें हैं. उनमें से मैंने ढूंढ कर एक अन्य उपन्यास “शिप्रा एक नदी का नाम है”, और पंकज बिष्ट की यायावरी की पुस्तक “खरामा-खरामा” के लिए आर्डर किया.
एक सप्ताह बाद बाहर से लौटा तो “मोनालीसा हंस रही थी” को पढने का लोभ संवरन नहीं कर पाया. यूँ तो उपन्यास पढ़ना इतना भी सरल नहीं है, जितना दिखता है, और ख़ास तौर से तब जबकि लेखक की पहली कृति से आपका वास्ता पडा हो. बहुत मन बनाना पड़ता है. पर एक बार जो शुरुआत को तो मन में जो सन्देश पहुँच रहे थे, न जाने क्यों वह इस उपन्यास के कुछ अद्भुत, दिल के करीब होने के लिए निश्चिंतता के फीलर्स संप्रेषित कर रहे थे.
एक दिन की दो सिटिंग में १२७ पृष्ठ की पुस्तक पढ़ डाली. ऐसा तभी पढ़ा जा सकता है, जब उसके सभी तत्व-- कथानक, शिल्प, भाषा और प्रस्तुतिकरण आपको उद्द्वेलित करें… अपील करें. यह बात हिन्दी साहित्य के विख्यात सृजक काशीनाथ सिंह की इस उपन्यास की समीक्षा के शब्दों में यूँ भी कही जा सकती है,
“ ‘मोनालीसा हंस रही थी’ देखा, खोला, पढना शुरू किया और पढ़ गया-- बिना रुके, बिना थके, एक सांस में. ना कहीं हांफना पड़ा, ना सुस्ताना पड़ा. इतना वक्त ही नहीं दिया मोनालीसा ने. ऐसे उपन्यास हों तो हिन्दी में पाठकों की कमी का रोना बंद हो जाए.”
उपन्यास में जिस प्रकार की भाषा के और बिंबों के माध्यम से कथानक प्रस्तुत किया है, वह संवेदनाएं तो जगाती ही, एक विशिष्ट किस्म का रोमांच भी पैदा करती है. जहाँ जरूरत है वहां लेखक को भाषा और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ऐसे दृश्य उत्पन्न करने में सफलता मिली है. न जाने कितने दृश्य ऐसे आये जब उपन्यास ने आँखों को नम करने, (नहीं… रुलाने) और धडकनों को असंयत करने का काम किया है. एक भी भाग ऐसा नहीं जिसकी उपयोगिता न हो. कई कहानियाँ समानांतर रूप से चलती हैं, पर एक दुसरे से गुंथी-बसी हुई. यही उपन्यास की सफलता का मानक है मेरे लिए.
व्यक्तित्व चित्रण का उदाहरण देखिये,
“प्रिंसिपल सतीश डंगवाल को इतना खुश कभी किसी ने नहीं देखा था. इतना भावुक होते हुए भी नहीं देखा था किसी ने उन्हें. यह पहाड़ पत्थर का नहीं, श्वेत खालिस बर्फ का बना हुआ था जो प्रेम और आत्मीयता की ऊष्मा से पिघलकर उल्लास की अलकनंदा बनकर बह चला था-- उस दिन.”
एक प्रसिद्ध कलाकार से कलात्मकता की जो उम्मीदें की जाती हैं, उस में अशोक भौमिक का यह उपन्यास इसलिए भी खरा उतरता है कि उन्होंने इसे अपनी सोच के अनुरूप प्रगतिशील कविताओं और अन्तर्राष्ट्रीय कला क्षेत्र की जानी पहचानी और कुछ अनाम हस्तियों के बिंबों से सजाया है. कहाँ लखनऊ के आर्ट्स कॉलेज के माली का एक टूटा हुआ सर्वेंट क्वार्टर, आजमगढ़ की गुमनामी और कहाँ मुंबई के लगभग फुटपाथी रहन-सहन से सम्भ्रान्त सोसाइटी में एक शानदार मकान में रहन-सहन. फिर लन्दन, पेरिस की कला-वीथियों की अनथक यात्रा. पर भौमिक सर ने अपने उपन्यास के सभी पात्रों को उनके अंतर्द्वंद्वों के साथ जिस तरह से जिया है, वह बिरले ही लोग कर पाते हैं. उपन्यास में कहीं कोई भटकाव नहीं है, अपेक्षाकृत अधिक पात्रों की मौजूदगी के.
किसी ईंट-मिट्टी-स्टील और सीमेंट की इमारत का इससे बेहतर विवरण क्या होगा,
“नेपियन्सी रोड़ के बंगले के फाटक को पार कर, जब किशन की गाडी अंदर दाखिल हुई तो किशन को लगा कि बँगला, लॉन और बगीचा एक महंगे गुलदस्ते की तरह बड़ी मेहनत से सजाया हुआ था. पर बावजूद इसके, एक ख़ामोशी थी जो वीरान, किसी परित्यक्त मकान की दीवारों जैसी एक अपरिचित अहसास बनकर चिपकी रहती है.”
“मोनालीसा हंस रही थी” कोई नया उपन्यास नहीं है. इसका प्रथम संस्करण २००७ में आया था. और जो मेरे हाथ में था, वह २०१४ का तीसरा संस्करण है. उपन्यास में जिस सामाजिक परिवेश की विद्रूपता को उकेरा गया है, उससे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी का वास्ता पड़ता है. किसी का कम किसी का अधिक, पर कितनी संवेदना के साथ हम उसे सहेज पाते हैं, अपने मन को स्थिर रख पाते हैं, यह कम ही लोग कर पाते हैं. और इस उपन्यास ने यह कर दिखाया है.
इसके पात्र एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते, कोई अतिक्रमण नहीं, फिर भी सम्प्रेक्षण में कहीं कोई कमी नहीं. जो वह दिखाना चाहते हैं पाठक उसे महसूस करता है, जैसे वह स्वयं सब कुछ घटित होते देख रहा हो. कॉर्पोरेट घरानों का दखल जिंदगियों को किस तरह किस मोड़ पर ला देता है, यह भी उपन्यास दिखाता है.
अन्तरंग स्थितियों को चित्रित करना किसी लेखक या कलाकार के लिए ऐसा होता है, जैसे दुधारी तलवार पर चलना. प्राय: लोग इस स्थिति में असंतुलित हो जाते हैं और भरभरा कर भौंतरी दीवार की तरह ढह जाते हैं, परन्तु यह सुखद है कि लेखक अंपनी सीमाओं और सामाजिक वर्जनाओं को इतनी खूबसूरती से शब्दों में पिरो देता है कि एक नशा… एक चमत्कार-सा लगता है, कि ऐसे भी बात कही जा सकती है. एक उदाहरण देखिये--
“जंगल के अंदर नशीले माँदल की आवाज सुनते हुए मीना और किशन, उस आवाज के उत्स को तलाशते, धीरे-धीरे बढ़ने लगे. घने दरख्तों वाले हरे घने जंगल के अंदर, भरी दोपहरी में शाम उतर आयी थी. पर कोई भी दीप कहीं भी नहीं जल रहा था.”
“आदिवासियों का माँदल न जाने कब थम गया था. मीना और किशन जंगल के काजल- हरे अँधेरे में अपना रास्ता खो चुके थे.”
एक दूसरे दृश्य में, तब जबकि कलाकार किशन अपनी निर्धनता से धनाड्य होने की यात्रा के महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर आ जाता है, उस दिन की एक तस्वीर देखिये,
“गैलरी से निकलकर अपने कमरे तक पहुँचते-पहुँचते रात काफी हो चुकी थी. जो कबूतर अब तक खामोश थे या रात के अँधेरे में गुटर-गूं-गुटर-गूं कर रहे थे. आहट पाकर फडफडाकर उड़ गये. फिर छत के ऊपर चक्राकार वे उड़ने लगे. किशन देर तक उन्हें देखता रहा. शहर की रात की रौशनी से उनके पेट और पैरों के नीचे के हिस्से चमक रहे थे, परों के ऊपर घना अन्धेरा था और उससे भी ऊपर काले कैनवास का शामियाना तना था.”
और अंत में जब किशन टूट चुका होता है, चूर-चूर हो गया था, उसे उन सब के चेहरे याद आ रहे थे, जो उसकी कला के साथ किये गये खेल के पात्र थे. तब उसे प्रिंसिपल प्रोफेसर अमित नियोगी भी दिखते हैं, एक ट्रैफिक लाइट पर. भले ही नींद में हो वह, और यह एक स्वप्न रहा हो, पर उनकी बढ़ी दाढ़ी और हाथ फैलाना, फिर हाथ की उँगलियों पर रंग के सूखकर गहराए धब्बे , और हथेली के बीचों-बीच बना एक सुराख-- सब कुछ उसे खुद से जुड़ता हुआ लगता है.
जब सहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्लेन आसमान के अँधेरे को चीरने लगा था, तब का दृश्य,
“चारों ओर जैसे कोहरा भर गया था. कोहरे के हलके नीले फैलाव के बीच ड्रिंक्स ट्राली को ठेलकर किशन की ओर आती लड़की एयर होस्टेस नहीं थी…. किशन ने चौंक कर देखा-- लीसा घेरारडीन! मोनालीसा!.... गहरा हरा लिबास-- खुले हुए बाल-- मोनालीसा उसके सामने खडी थी….”
“... मोनालीसा हंसने लगी. खिलखिलाकर वह बोली, ‘ख़ुदकुशी की बात मत करना-- आत्महत्या ज़िंदा लोग करते हैं. मरे हुए लोगों को खुदकुशी नसीब नहीं होती....”
“... मोनालीसा बिना कोई जवाब दिए शांत खडी रही…. होंठों पर एक हलकी हंसी लिए -- जो गालों से होकर गुजरती हुई-- पलकों पर पहुँच कर ठहर गई थी.”
“मोनालीसा हंस रही थी.”
यही था कथानक, “मोनालीसा हंस रही थी” का. दो-टूक पर सौम्य और बिंबों से उभर कर पर पूरी जिंदगी द्वंद्वों को जीते हुए अलग-अलग स्तरों पर खड़े इंसानों की एक कहानी. और हर मोड़ पर चमत्कृत करता हुआ अशोक भौमिक का लाजवाब लेखन.
बधाई अशोक भौमिक जी, आपका यह उपन्यास हमेशा याद रहेगा. “शिप्रा एक नदी का नाम है” थोड़ा अंतराल पर पढूंगा.